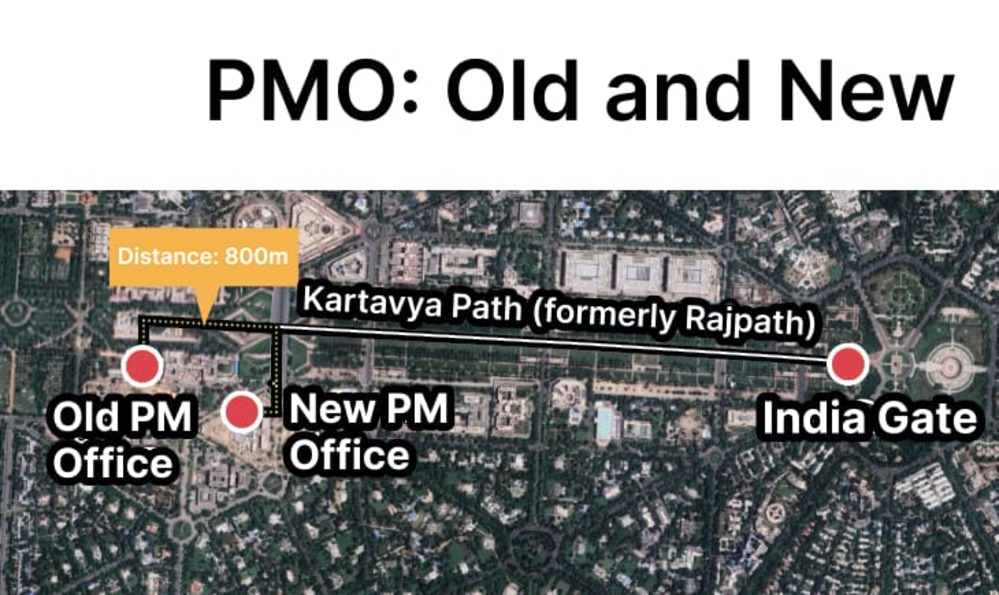– विजय गर्ग

स्वतंत्रता के बाद भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, लेकिन छात्रों में सीखने की समस्या अब भी बनी हुई है। शिक्षा की पहुँच भले ही बढ़ी हो, लेकिन बुनियादी साक्षरता का स्तर अब भी चिंताजनक है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) के अनुसार, कक्षा पांच के लगभग आधे छात्र दूसरी कक्षा के स्तर की सरल पाठ्य सामग्री पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं।
डाटा-आधारित मूल्यांकन की कमी
शिक्षा सुधार में डाटा-आधारित नीति निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है, लेकिन भारत इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। उदाहरण के लिए, 2009 में शुरू हुए अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) से दूरी बनाए रखना भारत को वैश्विक शिक्षा मूल्यांकन से दूर कर देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिना सुनियोजित मूल्यांकन और व्यवस्थित पाठ्यक्रम सुधार के कोई भी ढांचागत बदलाव प्रभावी नहीं हो सकता।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की भूमिका
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 ने इन कमियों को स्वीकार किया है और कई महत्वपूर्ण सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह नीति इस बात को रेखांकित करती है कि यदि शिक्षा प्रणाली अपने बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र में ही संघर्ष कर रही हो, तो उससे बेहतर परिणामों की अपेक्षा करना व्यर्थ है।
निजी स्कूलों की बढ़ती भूमिका
वर्तमान समय में, निजी स्कूलों की भूमिका शिक्षा सुधार में बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। सरकारी स्कूलों की गिरती गुणवत्ता और राज्य की सीमित भूमिका के कारण निजी स्कूलों ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी जगह बनाई है। आज कई राज्यों में 50% से अधिक छात्र निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
हालांकि, यह क्षेत्र अभी भी विखंडित और असंगठित है, जिससे नवाचार और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का समान रूप से प्रसार नहीं हो पा रहा है। निजी स्कूल अक्सर एक-दूसरे के सहयोग करने की बजाय प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे सफल मॉडल कुछ गिने-चुने संस्थानों तक ही सीमित रह जाते हैं।
निजी स्कूलों की पहल और नवाचार
कई निजी स्कूलों ने बहुभाषी शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम और वैश्विक संपर्क को अपनाकर छात्रों को एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ढालने का कार्य किया है। इसके अलावा, एड-टेक कंपनियों के सहयोग से कक्षाओं को तकनीकी रूप से सक्षम और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। लेकिन ये लाभ सभी छात्रों को समान रूप से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं।
सरकारी-निजी सहयोग की आवश्यकता
सरकारें अक्सर दीर्घकालिक ढांचागत सुधारों को प्राथमिकता नहीं देतीं, जिससे शिक्षा प्रणाली में बदलाव की गति धीमी हो जाती है। यहां निजी स्कूलों को आगे आकर शिक्षा सुधार में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
निजी स्कूलों को केवल अपने संस्थानों को बेहतर बनाने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि समूचे शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में भी योगदान देना चाहिए। इसके लिए उन्हें अपने आर्थिक हितों से परे जाकर सामाजिक जिम्मेदारी की भावना से कार्य करना होगा।
निजी स्कूलों को लेकर संदेह और उनकी जिम्मेदारी
हालांकि, निजी स्कूलों को अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यह धारणा काफी हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ निजी स्कूल केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि निजी क्षेत्र ने कई अन्य क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया है। ऐसे में, शिक्षा क्षेत्र को इस अपवाद में रखना उचित नहीं होगा।
एआई और टेक्नोलॉजी का उपयोग
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एड-टेक कंपनियों के सहयोग से शिक्षण को अधिक व्यक्तिगत, आकर्षक और प्रभावी बनाया जा सकता है।
निष्कर्ष
यदि हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करने होंगे। इसमें निजी स्कूलों की भूमिका केवल सहायक नहीं, बल्कि केंद्रीय होनी चाहिए।
शिक्षा सुधार के लिए निजी स्कूलों, एड-टेक कंपनियों और सरकार के बीच समन्वय आवश्यक है। यह साझेदारी प्रदर्शन और सामूहिक जवाबदेही के आधार पर होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि निजी स्कूल शिक्षा में नवाचार, डाटा-आधारित निर्णय और व्यापक परिवर्तन के केंद्र बनें, ताकि भविष्य की पीढ़ी को अधिक सक्षम और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके।
(विजय गर्ग, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, मलोट, पंजाब)