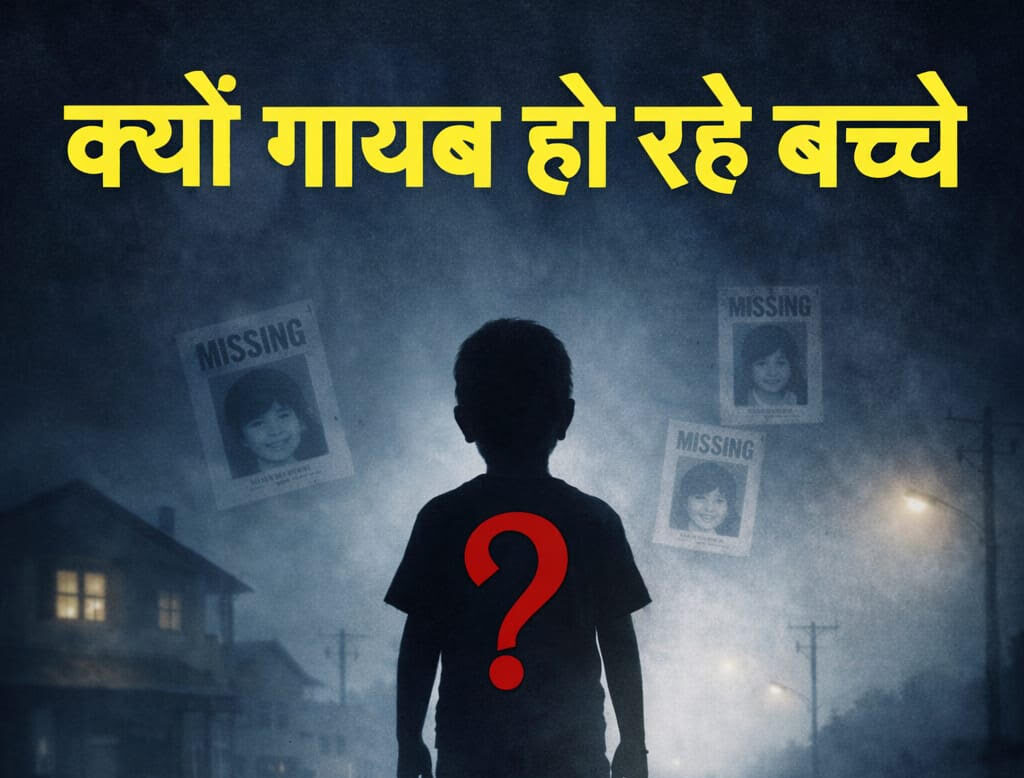सत्ता-संरक्षित अपराधों के सामने समाज, मीडिया और न्याय की सामूहिक परीक्षा
— डॉ. सत्यवान सौरभ

इतिहास के कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सभ्यता अपने ही आईने में झाँकने से डरने लगती है। आज हम ठीक उसी मोड़ पर खड़े हैं। जिन कांडों का खुलासा हो रहा है—जिनके वीडियो, दस्तावेज़ और गवाह सार्वजनिक हो चुके हैं—वे महज़ अपराध नहीं हैं, बल्कि मानवता के विरुद्ध सुनियोजित, संरक्षित और सत्ता-समर्थित हमले हैं। इन घटनाओं की भयावहता इतनी गहरी है कि शब्द भी लड़खड़ा जाते हैं। फिर भी समाज इन्हें “कंटेंट” की तरह उपभोग कर रहा है—चाव, रोमांच और क्षणिक घृणा के साथ—और फिर अगली सनसनी की ओर बढ़ जाता है।
यह कोई नई कहानी नहीं है। हर बड़े घोटाले, हर सामूहिक अपराध के बाद यही क्रम दोहराया गया है—पहले इनकार, फिर आंशिक स्वीकारोक्ति, उसके बाद माफ़ी या इस्तीफ़ा, और अंततः “कम्पैरिटिवली बेहतर” का आत्मसंतोष। मानो न्याय कोई तुलनात्मक पैमाना हो, जहाँ कम बुरा होना ही अच्छा होने का प्रमाण बन जाए। पर असली सवाल कहीं गहरा है—जब अपराध हो रहे थे, तब आत्मा कहाँ थी? क्या नैतिकता केवल कैमरों के सामने ही जागती है?
इन कांडों की सबसे भयावह परत सत्ता से जुड़ी है। उच्चतम पदों पर बैठे लोग—जिन्हें समाज ईश्वरतुल्य मानता है—जब दोषियों से संवाद करते, उन्हें संरक्षण देते, उनसे लाभ लेते या उनके लिए रास्ते बनाते पाए जाते हैं, तब लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाती है। यह व्यक्तिगत नैतिक पतन नहीं, बल्कि संस्थागत अपराध है। क्योंकि जब अपराध को व्यवस्था का संरक्षण मिलता है, तब वह अपवाद नहीं रहता—वह एक प्रणाली बन जाता है।
मीडिया की भूमिका यहाँ निर्णायक होनी चाहिए थी। लेकिन अक्सर वह भी दो ध्रुवों में बँटी नज़र आती है—एक ओर सनसनी, दूसरी ओर चुप्पी। सनसनी पीड़ितों की गरिमा को रौंदती है, जबकि चुप्पी अपराधियों को समय और सुरक्षा देती है। टीआरपी, क्लिक और ट्रेंड की दौड़ में सत्य दम तोड़ देता है। नतीजा यह कि जनता को तथ्य नहीं, भावनात्मक झटके मिलते हैं—और झटकों से स्थायी सामाजिक कार्रवाई कभी जन्म नहीं लेती।
क़ानून और जाँच एजेंसियों की स्थिति भी कोई आश्वस्ति नहीं देती। धीमी जाँच, अधिकार-क्षेत्र की उलझनें, राजनीतिक दबाव और अंतहीन प्रक्रियाएँ—ये सब मिलकर न्याय को टालने की एक सुव्यवस्थित मशीन बना देते हैं। कहा जाता है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान होती है; यहाँ यह कहावत एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आती है। पीड़ित थक जाते हैं, गवाह डर जाते हैं और अपराधी समय के साथ और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं।
सबसे असहज प्रश्न फिर भी आम जनता से जुड़ा है। क्या सचमुच हमें लकवा मार गया है? या हमें इस तरह ढाला गया है कि हम क्रोधित तो हों, पर संगठित न हो सकें? सोशल मीडिया हमें आवाज़ देता है, लेकिन दिशा नहीं। हम पोस्ट करते हैं, साझा करते हैं, गालियाँ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। वास्तविक दुनिया में उतरने का धैर्य, जोखिम और निरंतरता—ये सब दुर्लभ होते चले गए हैं।
यह भी एक सच है कि जनता को थकाने की बाक़ायदा रणनीति अपनाई जाती है। सूचनाओं की बाढ़, विरोधाभासी दावे, फर्जी खबरें और आधे-अधूरे सच—इन सबके ज़रिये भ्रम पैदा किया जाता है। और भ्रम से निष्क्रियता जन्म लेती है। निष्क्रिय समाज अपराधियों के लिए सबसे सुरक्षित वातावरण होता है।
कुछ देशों में माफ़ियाँ माँगी जा रही हैं, कहीं इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं और इन्हें बड़ी उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन माफ़ी तभी मायने रखती है जब उसके साथ जवाबदेही हो—क़ानूनी कार्रवाई, संपत्ति की जब्ती, नेटवर्क का खुलासा और स्थायी संस्थागत सुधार। केवल चेहरे बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती। इस्तीफ़ा न्याय नहीं है; वह अधिकतम उसकी शुरुआत हो सकता है।
इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक उपेक्षित पक्ष पीड़ितों का है। उनकी कहानियाँ, उनका दर्द और उनका पुनर्वास—सब कुछ हाशिये पर धकेल दिया जाता है। जबकि न्याय का अर्थ केवल सज़ा नहीं है; न्याय का अर्थ है पीड़ित की ज़िंदगी को दोबारा खड़ा करना। काउंसलिंग, चिकित्सा, शिक्षा, रोज़गार और गवाह सुरक्षा—ये सब उतने ही आवश्यक हैं जितनी अदालत की कार्यवाही। इनके बिना न्याय हमेशा अधूरा रहेगा।
तो रास्ता क्या है? प्रतिशोध नहीं। हिंसा की कामना हमें उन दरिंदों से अलग नहीं बनाती जिनसे हम घृणा करते हैं। सभ्यता की जीत क्रूरता से नहीं, बल्कि जवाबदेही से होती है। इसके लिए कुछ बुनियादी बिंदुओं पर समाज को एकजुट होना होगा।
पहला, स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय जाँच, क्योंकि सीमा-पार और सत्ता-समर्थित अपराधों में केवल राष्ट्रीय एजेंसियाँ पर्याप्त नहीं होतीं। दूसरा, पूर्ण प्रकटीकरण—नाम, पद, नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन का सार्वजनिक खुलासा। तीसरा, क़ानूनी सुधार—विशेष अदालतें, समयबद्ध सुनवाई और मज़बूत गवाह सुरक्षा क़ानून। चौथा, जिम्मेदार मीडिया, जो पीड़ित-केंद्रित, तथ्यपरक और निरंतर रिपोर्टिंग करे। पाँचवाँ, नागरिक एकजुटता—शांतिपूर्ण, संगठित और लगातार दबाव। क्योंकि बदलाव किसी एक पोस्ट से नहीं, बल्कि निरंतरता से आता है।
अंततः यह लड़ाई नैतिकता की है। हर समाज को कभी न कभी यह तय करना पड़ता है कि वह सुविधा चुनेगा या सत्य। सुविधा हमें सुला देती है, जबकि सत्य हमें बेचैन करता है—और इतिहास हमेशा उसी बेचैनी से आगे बढ़ता है। लानत दरिंदों पर तो बनती है। लेकिन इतिहास हमें इस आधार पर परखेगा कि क्या हमने अपने आक्रोश को क्षणिक नफ़रत में गँवा दिया, या उसे परिवर्तन की संगठित ताक़त में बदला। चुप्पी अब विकल्प नहीं है। देर से सही, पर न्याय आना चाहिए—और ऐसा न्याय, जो केवल दोषियों को दंडित न करे, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित बनाए।
यही इस समय की सबसे बड़ी माँग है। और यही हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी भी।
(डॉ. सत्यवान सौरभ, पीएचडी (राजनीति विज्ञान), एक कवि और सामाजिक विचारक है।)